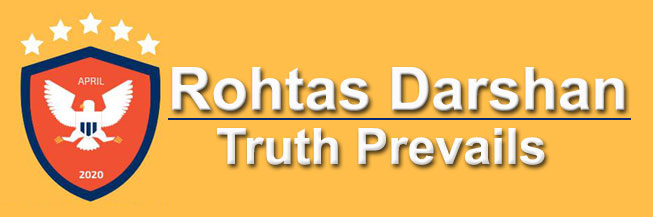रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : आनन्द का मूल स्त्रोत परमात्मा है ! अज्ञानतावश जीव ईश्वर की नित्य विद्यमानता को अनुभूत नही कर पाता अर्थात आत्मविस्मृति ही समस्त दुःखों की जड़ है। विवेक विचार से अभेदता प्राप्त कर आनन्द को चिरस्थायी बनाया जा सकता है ..! विपत्ति में विवेक-विचार और पुण्य कर्म ही सहायक बनते हैं। विवेक के आश्रय में जीने वालों को जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। विचारों के जमघट में हमें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनमें से कौन सा हित-कारक और कौन सा अहितकर, कौन सा करणीय और कौन सा त्याज्य एवं कौन से सही और कौन सा गलत है? इस स्थिति में कोई विशिष्ट शक्ति हमें निर्णय सुझाती है। मस्तिष्क की इसी निर्णायक शक्ति का नाम ‘विवेक’ है। यह हमारे अन्तरात्मा की वह पुकार है जिस पर हम सत् और असत् न्याय और अन्याय तथा अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं। उलझनों की अँधेरी घड़ियों में, चिन्ता के भयंकर क्षणों में यही विवेक हमारा पथ प्रदर्शन करता है। विवेक प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात रूप से वर्तमान रहता है। इस पर हमारे संचित और क्रियमान कर्मों की छाया का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह किसी में कम और किसी में अधिक दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम अपने संचित एवं क्रियमान कर्मों से इतने अधिक प्रभावित रहते हैं कि विवेक की पुकार हमें ठीक से सुनाई नहीं पड़ती। यही विवेक हमारी वास्तविक मानवता का प्रतीक और सद्बुद्धि का द्योतक है। इसके अभाव में मनुष्य पशु या उससे भी गया बीता बन जाता है और वह स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अन्ततः सृष्टि के लिए एक भार एवं अभिशाप हो जाता है …।
🌿 पूज्य “आचार्यश्री” जी ने कहा – व्यक्ति विचारों को ही कार्यरूप में परिणित करता है। जो कुछ व्यक्ति सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। विचारों की अस्वच्छता से उत्तेजना, असहिष्णुता, निष्ठुरता की पैशाचिक प्रवृत्तियां पनपती हैं, उन्हीं के कारण मनुष्य नरपिशाच तक बन जाता है। विचारों को संयमित करके व्यक्ति लौकिक और आंतरिक जगत में आनन्द का लाभ ले सकता है। विचारों के असंयम से ही मन, समय एवं धन का अपव्यय आरम्भ होता है। भौतिक जगत हो चाहे आत्मिक किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को अपव्यय की छूट नहीं है। धन की सार्थकता नेकी की कमाई में है और दूसरों के हित में अपने साधन लगाने में है। धन का अपव्यय या दुरुपयोग करना लक्ष्मी का साक्षात् अपमान है। अत्यधिक संचय अपव्यय सिखाता है। इसी से आडम्बर युक्त प्रदर्शन, फैशनपरस्ती, विवाहों में अनावश्यक व्यय किया जाता है। जुआ, मदिरा जैसे व्यसन घरों में पनपते हैं। विवेक के आश्रय में जीवन जीने वाला संयमित जीवन जीता है। संयमित और कर्तव्य-परायणता जीवन सुलभ और आनन्ददायक भी है। कर्तव्य पालन से पहले व्यक्ति को संयमी बनना पड़ता है। असंयमित जीवन-यापन करने वाले तिरस्कार और भर्त्सना के पात्र बनते हैं। कोई-कोई असफल होने पर ही श्रद्धा के पात्र होते हैं। केवल संयमशीलता एवं कर्तव्य-परायणता उन्हें यह स्थान दिलाती हैं। लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, शहीद भगत सिंह की जीवन गाथाएं इसके उदाहरण हैं। इसमें ऐसा कोई कारण नहीं कि मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण न कर सके। तो आईए, हम भी संयमशीलता एवं कर्तव्य-परायणता का स्वयं निर्वाह कर दूसरों को भी इस राजमार्ग पर चलने की सीख देकर मानव जीवन को सार्थक करें। यदि हमें अपनी और अपने समाज की आरोग्यता प्रिय है, यदि हम दीर्घजीवी होना चाहते हैं और अपने बच्चों को अकाल मृत्यु से ग्रस्त होने देना नहीं चाहते तो हमें संयम की प्रतिष्ठा करनी होगी। इसलिए अपने निज के स्वभाव में तथा घर के वातावरण में संयमशीलता को स्थान देना पड़ेगा, साथ ही असंयम से घृणा करनी होगी ..।